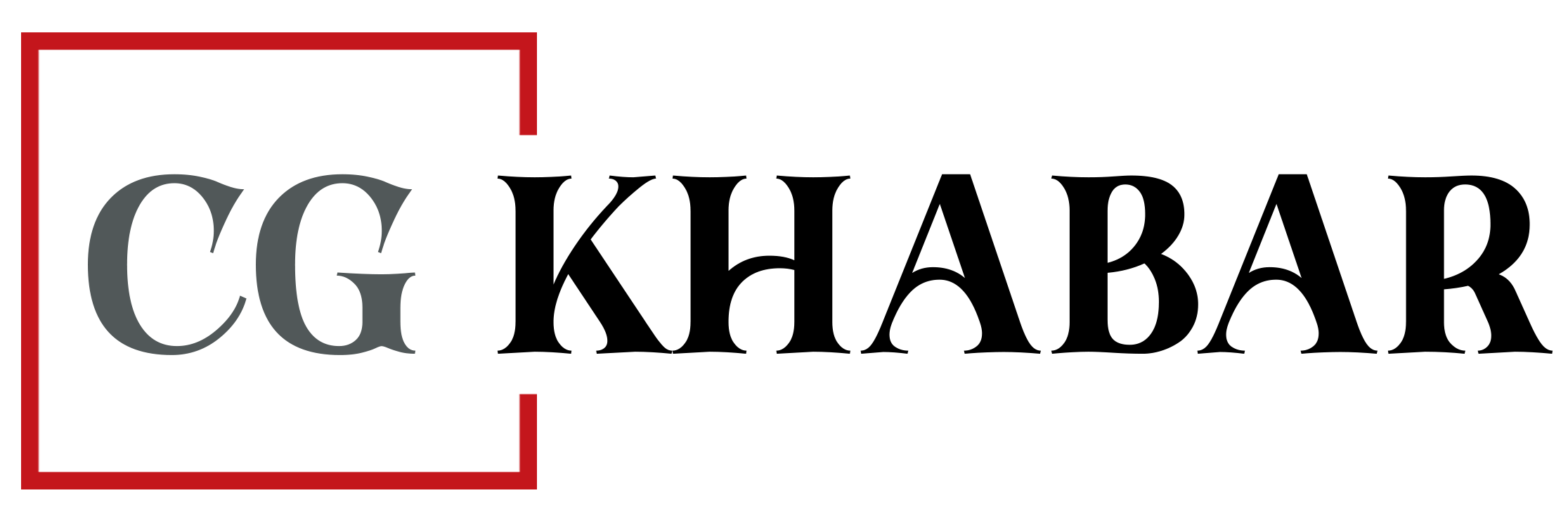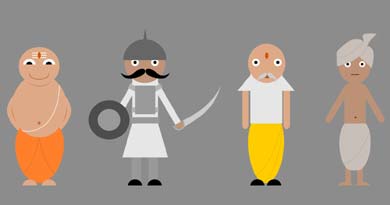क्योंकि जाति एक सच्चाई है
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जाति के आधार पर होने वाले अत्याचारों को रोकने वाले 1989 के कानून के मामले में जो निर्णय दिया, उसकी व्याख्या कई लोगों ने कानून को बेअसर बनाने की कोशिश के तौर पर की. इस अदालती निर्णय के बाद अग्रिम जमानत पर रोक लगाने वाला प्रावधान कमजोर हुआ है और एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच अनिवार्य हो गई है. इससे न्याय की गुहार लगाने की दलितों और आदिवासियों के उत्साह पर नकारात्मक असर पड़ेगा.
अपने मूल रूप में यह कानून दलितों और आदिवासियों को जाति के आधार पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है. न्याय की प्रक्रिया में मानवीय भूल से निपटने की व्यवस्था यह कानून करता है. लेकिन इस कानून के तहत सजा पाने वालों की संख्या काफी कम है. 2016 में अनुसूचित जातियों से संबंधित 89.7 फीसदी मामले अदालतों में लंबित थे. अनुसूचित जनजाति के मामलों में यह आंकड़ा 87.1 फीसदी था. ऐसा इसलिए था क्योंकि जानबूझकर कानून के प्रावधानों की अनदेखी की गई. उच्चतम न्यायालय ने क्या कोई ऐसा प्रावधान किया है जिससे प्राथमिक जांच जाति के आधार पर प्रभावित नहीं हो? क्या इसका एक मतलब यह नहीं निकलता दलितों में नैतिक बल कम है और उन्हें इसके दुरुपयोग के लिए संदेह की नजर से देखा जा रहा है?
प्राथमिक जांच का आदेश देकर सर्वोच्च अदालत नैतिक समस्या का समाधान कानूनी ढंग से करना चाह रही है. अदालत को इस समस्या को पूरे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए. इस गिरावट को गुजरात के उना में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जरिए देखा जा सकता है.
न्याय तंत्र खुद को अलग रखने के रवैये को दंडात्मक नहीं मानता. ऐसा इसलिए कि भीड़ को नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को कोई सामाजिक अपराध या कोई नैतिक अपराध या फिर किसी कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग का कसूरवार माना जाता है. इसलिए प्राथमिक जांच के आदेश को यह कहते हुए सही ठहराया जा रहा है कि इससे दुरुपयोग बंद होगा और अरोप लगाने वाले और अरोपित दोनों को बराबरी का अवसर मिलेगा.
एक व्यक्ति को केंद्र बनाकर कानूनी व्यवस्था की रचना समाज के एक वर्ग में सही मानी जा सकती है लेकिन इसकी दो बुनियादी समस्याएं हैं. पहली बात यह कि दुरुपयोग के भय से हर मामले को संदेह की दलदल में धकेल दिया जा रहा है. इससे जाति आधारित अपराधों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.
दूसरी समस्या अदालत के निर्णय से जुड़ी हुई है. अदालत ने कहा कि आरोप लगाने वाला और आरोपित दोनों कानून की किताबों के बाहर की ताकतें हैं. ऐसे में किसी खास इलाके में गैर-दलित जातियां ताकतवर बने रहना चाहेंगी और इससे कुछ मौकों पर दलितों को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ सकता है कि वे कानून का दुरुपयोग करें.
क्या इस कानून की नैतिकता को अपनी पीठ पर ढोने का बोझ दलितों को ही उठाना है. नैतिक तौर पर देखें तो कानून दलितों में एक नाराजगी का भाव ला रहा है. इसलिए हमें यह राय नहीं बनानी चाहिए कि दलितों में इस कानून के दुरुपयोग का रुझान है.
हमें यह भी पूछना चाहिए कि इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी परिस्थितियां कौन मुहैया करा रहा है. अगड़ी जाति के लोग अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं और इसी कोशिश में अत्याचार होते हैं. इसलिए यह गैर-दलित जातियों की जिम्मेदारी है कि वे किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना को खत्म करें. अगर जाति सच्चाई नहीं अफवाह होती तो इस तरह के कानून की कोई जरूरत ही नहीं होती. जाति अधिकांश भारतीयों के लिए एक आदत की तरह है तो इस कानून के कठोर प्रावधानों का आश्रय लेना अपरिहार्य होता रहा है.
अदालत का निर्णय कानून पर आधारित है लेकिन इसे पूरे समाज की नैतिकता को अभिव्यक्त करने वाला बनना चाहिए. ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा कि भारतीय कानूनी तंत्र इस जरूरत को लेकर असंवेदनशील रहा है. प्रगतिशील न्यायिक सक्रियता को समाज की सामूहिक अभिव्यक्ति बनना चाहिए. अल्पकालिक राय यह हो सकती है कि मूल कानून के तहत दलितों को जो अधिकार मिले थे, उसे छीना जा रहा है. लेकिन इससे सामूहिक नैतिक सोच की प्रगति में बाधा पैदा होगा जो सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है.
1966 से प्रकाशित इकॉनोमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली के नये अंक का संपादकीय