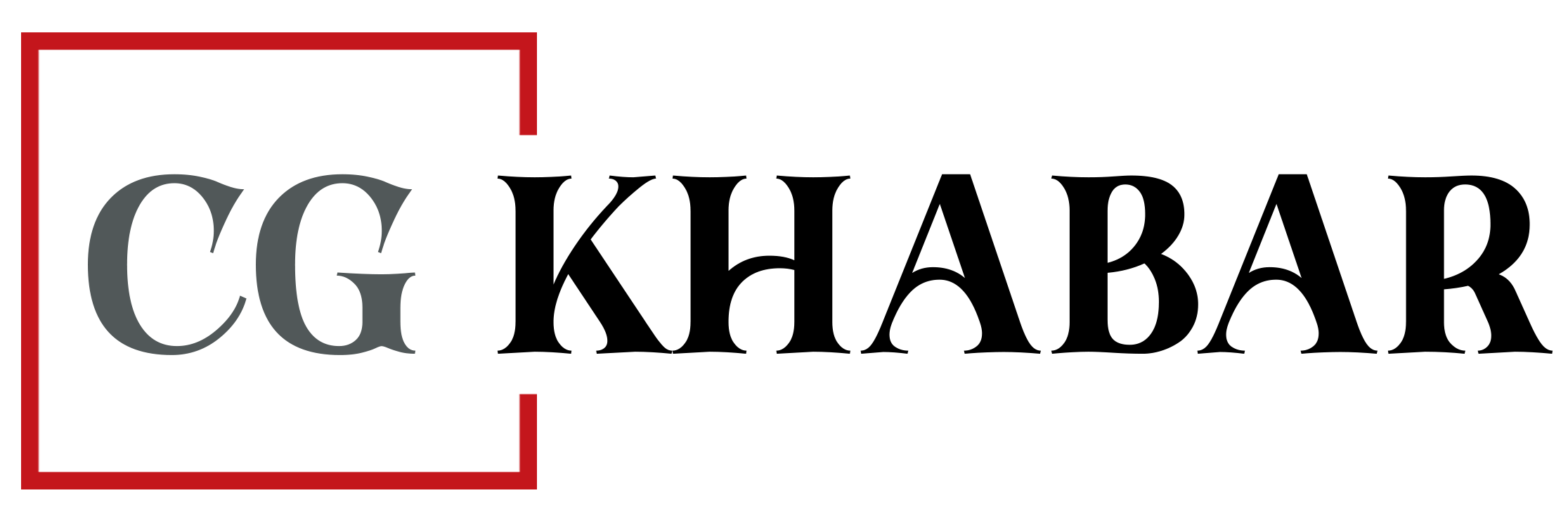लोकतंत्र से भीड़तंत्र की ओर
अभी के भारत में ‘कानून का राज’ की जगह भीड़तंत्र ले रही है. यह बेहद परेशान करने वाला है कि भारत में भीड़ द्वारा किए जाने वाले हमले सामान्य होते जा रहे हैं. समाज के बड़े वर्ग से इसकी जो आलोचना होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है. इसके उलट इस तरह की हिंसा का लोग साथ दे रहे हैं. न्यायपालिका इसके लिए राज्य सरकारों और कानूनी मशीनरी को जिम्मेदार ठहरा रही है.
भीड़ द्वारा किए जाने वाले हमलों के जरिए कानूनी दायरे से बाहर सजा देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. बलात्कार के उन मामलों में यह अधिक दिख रहा है जिनमें पीड़ित किसी प्रभावी सामाजिक पृष्ठभूमि की हो. अभी हाल ही में यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिखा. यहां आठ साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है और हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा तब और बढ़ा जब उन्हें यह शक हुआ कि कसूरवार मुस्लिम समाज के हैं.
ऐसे ही घटना 1 जुलाई को महाराष्ट्र के धुले में हुई जिसमें पांच लोगों को मार दिया गया. हमें यह समझना होगा कि हर ऐसी घटना पहले से योजना बनाकर नहीं होती. न ही जनता उन्हें वस्तुनिष्ठ होकर देखती है. सोशल मीडिया के जरिए इन घटनाओं को भड़काया जाता है. इन सबके बावजूद ऐसी घटनाओं को सही नहीं कहा जा सकता. कानून अपने हाथ में लेकर सजा देना सही नहीं है. हालांकि, कुछ मामलों में पुलिस और लोगों ने भीड़ के हमलों से भी लोगों को बचाया है. उत्तराखंड में मई, 2018 में पुलिस ने एक व्यक्ति को बचाया और मालेगांव में स्थानीय लोगों ने पांच लोगों जिनमें एक महिला भी शामिल थे, उन्हें भीड़ से बचाया.
भीड़ द्वारा किए जाने वाले हमलों की कुछ वजहें हैं. पहला है पुलिस और न्यायपालिका की नाकामी की वजह से उपजा पूर्वाग्रह और इससे पैदा हुई सामूहिक असुरक्षा की भावना. उदाहरण के लिए अप्रैल 2017 में पहलू खान पर तथाकथित गौरक्षकों द्वारा किया गया हमला या ऐसा ही कोई और मामला लें, इनमें हमला एक समुदाय के प्रति आशंका की वजह से हुआ है.
बलात्कार के आरोपियों को मारकर टांग देना जाति और समुदाय के प्रति प्राथमिक प्रतिबद्धता को दिखाता है. जाति और संप्रदाय से जुड़ी चीजें कानूनी जागरूकता को प्रभावित कर रही हैं. खास तौर पर तब जक पीड़ित और आरोपी दोनों की सामाजिक पहचान जाहिर हो जाए. अगर आरोपी पीड़ित से अलग जाति का है या फिर दलित या मुस्लिम है तो प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो जाती है. यह महाराष्ट्र के खैरलांजी में 2006 में दलित नरसंहार के मामले में भी दिखा था. अगर पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय से हो तो न सिर्फ प्रभावी सामाजिक वर्ग में कानून के प्रति निरादर दिखता है बल्कि कानून के रक्षकों में भी यही भाव दिखता है. जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या का मामला इसका उदाहरण है.
वहीं दूसरी तरफ अगर पीड़ित गैर-दलित या गैर-मुस्लिम समाज से हो तो इन वर्गों के लोगों में त्वरित न्याय हासिल करने का भाव जग जाता है. यह 2016 में महाराष्ट्र के कोपारडी गांव और मंदसौर की घटना से जाहिर होता है. कोपारडी में पीड़ित और आरोपी एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि के थे और महिलाओं ने टीवी चैनलों पर आकर आक्रामक ढंग से अपनी बात रखी. मंदसौर में भी यही हुआ. इससे बहुसंख्यक समाज ‘चित भी मेरी और पट भी मेरी’ के सिद्धांत पर चलता दिख रहा है.
इन सबसे यह पता चलता है कि पीड़ित की सामाजिक और धार्मिक पहचान जितनी करीब होगी, कानून का राज उतना ही दूर होगा. अगर आरोपी की सामाजिक दूरी कम है तो कानून से दूरी कम होगी. जाति और सांप्रदायिक सजगता भारत में एक ही तरह के हैं. जाति और संप्रदाय के प्रति जितनी अधिक चेतना होगी, कानूनी चेतना उतनी ही कम होगी. वहीं अगर जातिगत चेतना कम होती है तो कानून का प्रभाव उतना अधिक होगा.
लेकिन दोनों ही मामलों में भीड़ के जरिए न्याय देने की सोच कानूनी ढांचे के साथ खिलवाड़ है और इससे अंततः लोकतंत्र का भविष्य नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो रहा है.
1966 से प्रकाशित इकॉनोमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली के नये अंक का संपादकीय