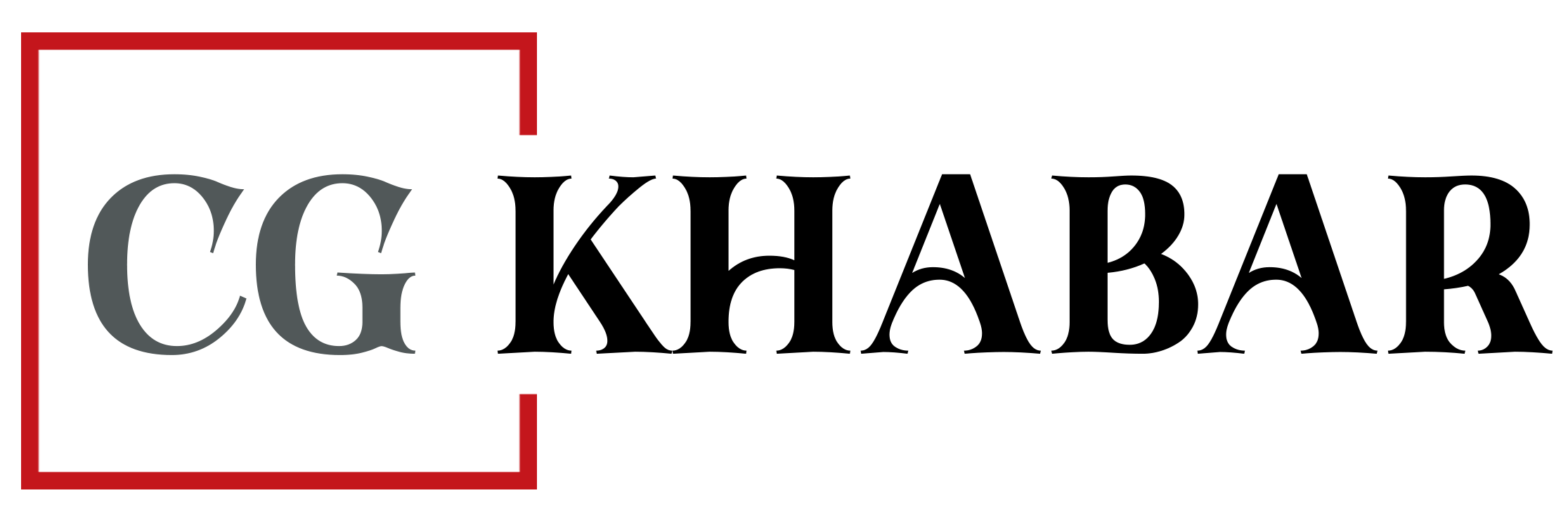मीडिया में वर्चस्व का चश्मा
अनिल चमड़िया
मैंने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम पन्द्रहेक साल पहले एक पत्र लिखा. उसमें मैंने बताया कि भारत के समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें बड़े पैमाने पर छपती रहती हैं कि इस्लामिक देशों में महिलाओं के साथ किस तरह का नृशंस व्यवहार होता है. उन देशों में कितनी धार्मिक कट्टरता है. उस लंबे पत्र में कई उदाहरण दिए गए थे. लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जातीय उत्पीड़न की घटनाओं की खबरें नहीं आती हैं, बड़ी तादाद में वहां की महिलाओं को प्रति वर्ष बड़ी संख्या में दुनिया भर के वेश्यालयों की तरफ धकेल दिया जाता है और वह दुनिया के सबसे गरीब देश में एक है. जबकि वह दुनिया का एक मात्र हिन्दू राष्ट्र है और वहां भारत की तरह गुलामी के हालात भी नहीं पैदा हुए. मैंने राजनीतिक पार्टियों से ये पूछा था कि वे अपने स्तर से हिन्दू राष्ट्र नेपाल में उत्पीड़न के सवालों को क्यों नहीं उठाते हैं.
इस तरह मीडिया की भूमिका को दो तरह की घटनाओं की तुलना करके यह दावा किया जा सकता है कि वह एक की तुलना में दूसरे को कितनी अहमियत देता हैं. मुझे कुछ दिनों पहले ही एक शोध पत्र मिला, जिसमें कुछेक घटनाएं दलित उत्पीड़न की थी और कुछेक घटनाएं वैसी थी जिन्हें समाचार पत्रों में मुस्लिम उत्पीड़न की घटनाओं के रुप में जगह मिल रही थी. उस अध्ययन में यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं से कहीं ज्यादा महत्व मुसलमानों के खिलाफ होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को मिल रहा है. ऐसा नहीं था कि ये जो अध्ययन करने वाली संस्था थी, वह दलितों की शुभचिंतक थी. वह जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों की संस्था मानी जाती है और उसने उस वक्त इस तरह के अध्ययन को अपने राजनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण समझा जब कि दलित और मुस्लिम के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा था.
शोध को सत्य की खोज नहीं माना जा सकता है. सत्य सापेक्ष होता है. यहां जापान की बेहद चर्चित फिल्म रशोमोन (1950) की चर्चा जरूरी हो जाती है, जिसमें फिल्मकार ने एक ही घटना को कई तरह से प्रस्तुत किया है और जिस भी तरह से वह घटनाएं प्रस्तुत की गई, वे बिल्कुल सच लगती हैं. फिल्म की बुनावट इस प्रकार है कि उस घटना से जुड़ा हर पात्र अपने तरीके से उस घटना को प्रस्तुत करता है और अपनी प्रस्तुति में खुद को छोड़कर दूसरे पात्रों को कटघरे में खड़ा करता है.
यदि राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को लेकर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका हर किरदार अपने तरीके से अपनी राजनीति में धर्म को जरुरी मान सकता है और उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित कर सकता है. भिन्नताओं के भरे समाज में वर्चस्व स्थापित करने की राजनीतिक होड़ एक धर्म की राजनीति दूसरे धर्म या धर्मों को कटघरे में खड़ा किए बिना आगे बढ़ नहीं सकती है. लेकिन जहां धर्म की राजनीति से अलग सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राजनीति होती है तो वहां किसी भी घटना को देखने की दृष्टि भिन्न हो जाती है.
हमारे समाज में यह एक प्रवृति तेजी के साथ बढ़ी है कि किसी भी स्थिति को दो छोर पर खड़ा करके उसकी तुलना की जाए. जैसे साम्प्रदायिक दंगे हों तो यह आंकड़ा प्रस्तुत किया जा सकता है कि भाजपा के शासनकाल में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए और उससे कितने ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए. यानी दंगे के कम और ज्यादा होने की वजह के रुप में शासन के तौर तरीकों को रखकर इस बहस को यह दिशा दी जा सकती है कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण क्या हैं और इससे किसके हित पूरे होते हैं?
मीडिया को दो नजरिये से कटघरे में खड़ा किया जा सकता है. एक तो नजरिया यह हो सकता है कि अपनी राजनीति के अनुकूल कैसे मीडिया में खबरों के लिए जगह बनाने का एक दबावमूलक वातावरण तैयार किया जाए. दूसरा नजरिया यह हो सकता है कि मीडिया जिन तरह की खबरों को अनदेखा करता आ रहा है, वैसी खबरों के लिए जगह बनाई जाए ताकि राजनीतिक पार्टियां आर्थिक व सामाजिक स्तर पर यथास्थितिवाद की पक्षघरता की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए बाध्य हों. मीडिया में खबरों की जगह बनने के मसले को समझना बहुत पेचिदा काम हैं. एक तो मीडिया संस्थानों का अपना एक आर्थिक लक्ष्य होता है और वह संस्था अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने प्रकाशन व प्रसारण को राजनीतिक दबाव के माध्यम के रुप में इस्तेमाल करता है.
दूसरा राजनीतिक स्तर पर मीडिया में ये दबाव बनाने की कोशिश होती है कि वह उसके लक्ष्यों को हासिल करने में उसका साझीदार बनें. दुनिया का कोई भी मीडिया संस्थान यह दावा नहीं कर सकता है कि वह समाज के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं. पूंजीवादी समाज में मीडिया आर्थिक और सामाजिक स्तर पर प्रभाव रखने वाले वर्गों के हितों में होता है. लेकिन वहां एक यह संघर्ष चलता है कि वह किस तरह के सामाजिक मूल्यों के साथ लंबे समय तक खुद को कायम रख सकता है.
भारतीय समाज में मीडिया पर सामाजिक और आर्थिक स्तर पर वर्चस्व रखने वालों की पक्षघरता को लेकर कई शोध सामने आ चुके हैं. हाल के वर्षों में मीडिया पर यह दबाव लगातार बना हुआ है कि वह संविधान के उस मूल्य को छोड़ दें जिसे धर्म निरपेक्षता के रुप में स्थापित किया गया है. इसीलिए जब वैसी घटनाएं होती हैं, जिनका राजनीतिक स्तर पर असर होता है तो दो घटनाओं को सामने रख दिया जाता है.
मसलन जम्मू के कठुआ में नाबालिग के विरुद्ध बलात्कार और हत्या और मध्य प्रदेश के मनसौर में नाबालिग के विरुद्ध बलात्कार की घटनाओं को सामने रख दिया गया क्योंकि एक के बलात्कारी को हिन्दू मान लिया गया और पीड़ित को मुसलमान और दूसरी घटना में पीड़ित को हिन्दू और बलात्कारी को मुसलमान मान लिया गया. साम्प्रदायिक दृष्टि से इन दोनों घटनाओं के बीच और उनके खिलाफ प्रतिक्रियाओं की तुलना करें तो किन किन तथ्यों को छुपाया जा सकता है.
पहला तो यह छुपाया जा सकता है कि दोनों ही राज्यों में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी का नाम एक ही है. दूसरा, बलात्कार की संस्कृति के विस्तार के कारणों की तरफ से ध्यान दूसरी तरफ हटाया जा सकता है.
इसी तरह ईसाईयों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं को लेकर ये कहा जा सकता है कि मीडिया में उसे पर्याप्त जगह नहीं मिली. बिल्कुल यह सच लग सकता है. लेकिन ठीक उसी तरह से उसने इस सच्चाई को भी पर्याप्त जगह नहीं दी कि लाखों की संख्या में गरीब गूरबे और आदिवासियों को दूर दराज के जंगल में जाकर पहली बार ईसाईयों ने ही स्कूल के दर्शन करवाएं. डा. राम दयाल मुंडा ने एक किताब आदिवासी अस्तित्व व झारखंडी अस्मिता के सवाल में बताया है कि कैसे आदिवासियों का हिन्दूकरण किया गया है. लेकिन उसे भी पर्याप्त जगह अब भी नहीं मिलती है. अपने वर्चस्व के चश्मे से देखने से सच की कई परतें दबी रह जाती है.