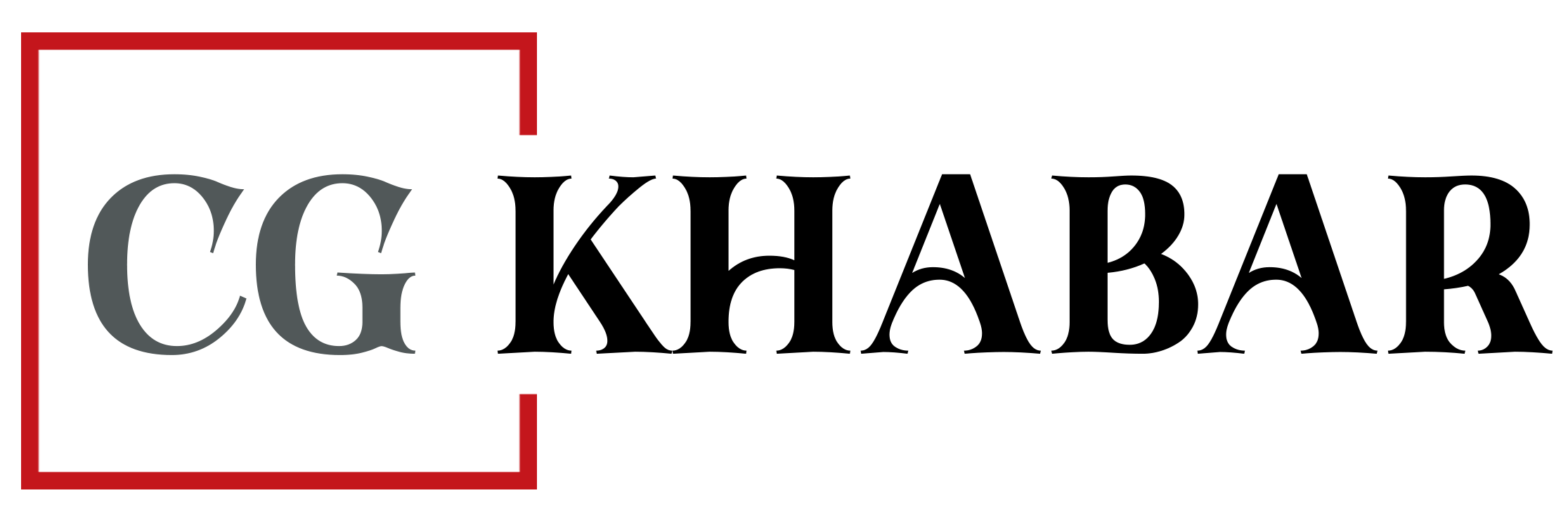इस ड्रैकुला को पहचानते हैं आप?
डॉ. विक्रम सिंघल
पश्चिम विशेषकर हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें मध्ययुगीन यूरोप की एक लोककथा से परिचय कराया है, जो 1897 में प्रकाशित ब्राम स्ट्रोकर के उपन्यास ‘ड्रैकुला’ के बाद कहीं अधिक चर्चा में आई थी. इस लोककथा में एक ऐसे खलनायक का उल्लेख है, जो न तो जीवित है और ना ही मृत. उसका जीवन औरों के शरीर से जीवन उर्जा सोखकर चलता है और इसके लिए वो दूसरों का खून पीते हैं.
यहां तक की कहानी तो दुनिया भर में आम है लेकिन इस कहानी का अगला हिस्सा अलग है. इस अलग कहानी में ये होता है कि जिसे भी यह वैम्पायर या पिशाच ख़ून पीने के लिये काटता है, वह मनुष्य भी पिशाच में बदल जाता है. इस कहानी की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सवा सौ साल बाद भी लगभग हर साल इस कहानी पर फ़िल्में बन रही हैं. स्टेफेनी मेयेर की ट्वाईलाईट श्रृंखला लंबे समय से, सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास है. इसके भोंडे रूपांतर भारतीय टेलीविज़न पर भी काफी लोकप्रिय हुए हैं.
हैदराबाद में बलात्कार के चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ में मारे जाने की घटना के बाद जिस तरीके से इसका सोशल मीडिया में उसका स्वागत किया गया, मुझे अनायास ड्रेकुला की याद आ गई. तो क्या हमारी राजनीतिक और सामाजिक चेतना का भी पैशाचीकरण हो गया है?
पिछले कुछ सालों में लिंचिंग या भीड़ द्वारा घेर कर की जाने वाली घटनाओं में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है. कभी गौ तस्करी के नाम पर तो कभी गौ मांस के नाम पर तो कभी बच्चा चोरी का आरोप लगाकर लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया. 2014 में पुणे में मोहसिन शेख की भीड़ द्वारा हत्या की घटना के बाद, दादरी में अख़लाक़ के घर में घुस कर गौ मांस खाने के आरोप में उसी के पड़ोसियों द्वारा उसकी पीट पीटकर हत्या किये जाने की घटना की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी.
इसे एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव या षड़यंत्र के रूप में देखा गया, जहाँ लोगों ने तर्क दिया कि संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों में वैकल्पिक न्याय व्यवस्था की वैधता स्थापित करने के लिए साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है. इस तर्क को बल मिला, जब सत्ताधारी दल के नेता और सांसद हत्यारों के समर्थन में उतर कर सामने आये. इसके अलावा और भी तर्क आये कि यह एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकित करने की योजना का हिस्सा है. साजिश को लेकर तर्क दिया गया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और संविधान उनकी रक्षा नहीं कर सकते और उसके लिए उन्हें, उस विशेष दल और उसके नेताओं का संरक्षण प्राप्त करना होगा. यह एक राजनीतिक उपक्रम भी लगने लगा, जब किसी समुदाय के कुछ लोगों, विशेषकर युवाओं को इसमें संलिप्त करके, उन्हें कानूनी रूप से आपराधिक मुक़दमे में फंसा कर, उन्हें अपनी रक्षा के लिए उसी व्यवस्था का मोहताज बना दिया जाये, जिससे वह पूरा समाज उनका राजनीतिक बंधक बन जाये.
जब राजसमंद में शंभूलाल रेगर ने मोहम्मद अफराजुल की हत्या का विडियो बनाकर उसे वायरल किया तो उसने मान लिया था कि वह उस विमर्श और व्यवस्था में एक पायदान और ऊंचा पहुंचने वाला है. शंभूलाल इसमें सफल भी हुआ. एक भीड़ ने उसके समर्थन में प्रदर्शन करते हुए न्यायालय के ऊपर फहराये हुए तिरंगे को भगवा झंडे से बदल दिया और गणेश और दुर्गा झांकियों में उसके पुतले बनने लगे. इंटरनेट पर उसके लिये धन एकत्र किया जाने लगा और शंभूलाल को चुनाव मैदान में उतारने के लिये अभियान शुरु किया गया.
इस घटना के निहितार्थ समझें तो दीवार पर लिखी इबारत की तरह बहुत साफ़ नज़र आ रहा था कि राज्य और कानून के निष्फल होने का आभास लोगों में सफलतापूर्वक पहुँचाया जा चुका है और लोग वैकल्पिक व्यवस्था में अपने लिए अच्छी सीट आरक्षित कर लेना चाहते हैं. अक्सर इस तरह की योजनाएं अपने लक्ष्य पर रूकती नहीं हैं और उससे आगे निकलती चली जाती हैं. दीमापुर और कारबी आंगलोंग की वारदातें तो कम से कम यही बताती हैं. भीमा कोरेगांव जैसी घटनायें भी उसी का हिस्सा लगती हैं, जहां हो सकता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो लेकिन फौरी तौर पर यह तो बहुत साफ़ समझ में आता है कि इस तरह से एक पूरे वर्ग और पहचान को उनकी बेबसी का अहसास कराया जाये, जहाँ पीड़ित को ही आक्रांता बना दिया जाये और उन्हें न तो राज्य, और कानून से न्याय की उम्मीद रहे और ना ही समाज से सहानुभूति की.
इस पूरे परियोजना का एक सामाजिक आधार भी है, आखिर संविधान का महत्व क्या होता है. संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, जो समाज के सभी वर्गों को आश्वस्त करता है कि न्याय और प्रगति के मूल्यों को साधते हुए, उनके विशेष हितों की रक्षा करेगा और राज्य व्यवस्था के लिए वह आवश्यक आम सहमति तैयार करता है. गरीब और पिछड़े बहुमत को सामाजिक न्याय और प्रगति के अवसर सुनिश्चित करना ही इसका आधार होता है. ऐसे में संपन्न और अगड़े वर्गों को अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए इसी संविधान को शिथिल करना जरूरी हो गया. इसके लिए न सिर्फ जनता का संविधान पर से विश्वास का उठना जरूरी है बल्कि यह भी कि उस सहमति को भी तोड़ा जाये, जिसे संविधान ने स्थापित किया था और जो लोकतंत्र का आधार होता है.
इसके लिए सामाजिक विद्वेष खड़ा करना ज़रूरी है, जिसमें धार्मिक विसंगतियां बहुत सहायक होती हैं. लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या बाकी रह जाती है. वो है लोगों की संवैधानिक मूल्यों पर आस्था, जिसका आधार समाज के मूख्य नैतिक मूल्यों पर स्थापित होता है, और भारत के सन्दर्भ में यह अहिंसा और अपरिग्रह के रूप में पहचाने जा सकते हैं. तो इन मूल्यों के विरुद्ध हिंसा और संग्रह या उपभोग को मूल्य बना कर स्थापित करना भी आवश्यक है. अब रास्ता साफ़ है, लोगों को पहले उपभोक्ता बनाओ और फिर हिंसक सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही ध्वस्त हो जाएँगी.
एक बार फिर हम लौटते हैं अपने ड्रैकुला और पिशाचों की किंवदंतियों पर. दुनिया की हर संस्कृति में ऐसी सत्ता की कल्पना पायी जाती है, जो आत्मा विहीन या अजीव होते हैं और यह उनके अमर होने के साथ ही नैतिकता से भी स्खलित होने का प्रतीक है. सामान्य जीवन में व्याप्त सभी नैतिक मूल्यों से विहीन एक शक्तिशाली व्यक्तित्व या विचारधारा जो रक्त से पोषण पाती हो, इसी किरदार का विस्तार है.
अब अगर विचारधारा एक सांकेतिक काया लिए हुए है तो उसका रक्तपान भी सांकेतिक ही होगा. यदि एक विचारधारा हिंसा को नैतिक मूल्य की तरह स्थापित करे, उसके लिए कमजोर शत्रुओं का निर्माण करे, असुरक्षा और
अनिश्चिंतता को बढ़ाये और उसे राष्ट्र, धर्म रक्षा से जोड़े तो वह इतिहास में अपने लिए प्रतीक व्यक्तित्वों को भी गढ़ता है, जो अक्सर झूठा होता है. इस तरह वह अपने आप अमर होने का दम्भ भी भरे तो उसके पिशाच बनने में अब दो ही कमियां रह जाती हैं- रक्तपान और लोगों को संक्रमित करने की क्षमता.
हम सब जानते हैं बहते खून की प्रतीकात्मक क्षमता, जो यदि अपना हो तो करुणा और गैर का हो तो क्रूर आवेश का संचार करती है. संचार क्रांति के युग में यह और भी सहज है, जहां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा सोशल मीडिया तक, अब बेनामी खबर या विचार, किसी नियम या मर्यादा की मोहताज़ नहीं है. तो इस पिशाच को हर दिन खून की खुराक चाहिए और इसका ठेका इसने मीडिया को दे दिया है. खून मीडिया में रोज़ मिलना चाहिए,चाहे किसी अपने का हो या दुश्मन का. चाहे लिंचिंग हो, रेप हो, एनकाउंटर हो या युद्ध ही क्यों न हो और न हो तो तो दुर्घटना भी चलेगा लेकिन बहता खून ज़रूर होना चाहिए.
किसी कुकरी शो की तरह पाकिस्तान के साथ हो सकने वाली युद्ध या रक्तपात के आम दावत को दिखाया जाता है जहाँ अलग-अलग खाना पकाने की विधियों की जगह हथियार और युद्ध के संभावित परिणाम गिनाये जाते हैं. टॉक शो के ज़रिये अफवाहों और ‘फेक न्यूज़’ के जरिये हमारे समय का यह पिशाच लोगों को काटता है कि यह संक्रमण वहां तक पहुंचे. कितना आरामदायक है कि आपको अपना भोजन न कमाना है न खोजना, वो रोज आपके घर में या फिर जेब में रखे फ़ोन पर नियम से पहुंचा दिया जाता है.
जब विचारधारा सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि व्यवस्था को भी चपेट में ले ले तब हमें कश्मीर, बस्तर, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद नज़र आते हैं. 70 लाख कश्मीरियों की हालत दिखा कर कहा जाता है कि अंदाज़ा लगाओ पकवान कैसा होगा. व्यवस्था भी हमारी हमखुराक है. मुठभेड़ों में पुलिस के वरिष्ठ अफसर एक दुसरे से ‘स्कोर’ पूछते हैं, और ‘अब तक छप्पन’ जैसे फ़िल्में बनती हैं.
हैदराबाद में हुई घटना की खबरें, पहले बलात्कार और फिर पीड़िता की नृशंस हत्या, फिर उसपर मीडिया का तूफ़ान जिसमें नेता अभिनेता सभी वीर अपनी उत्तेजना का प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद पुलिस का फ़ौरन चार लोगों को गिरफ्तार करके केस को सुलझा लेना, दूर की कौड़ी लाने वालों को, बिगड़ती अर्थव्यवस्था में लोगों को व्यस्त रखने का जरिया लग रहा था.
लेकिन जब उसी इंटरनेट पर उस रेप के वीडियो को 80 लाख लोग खोजते हैं तो समझ में आता है कि यह तो एक बहुत भूखे पिशाच की बात हो रही है. एक तो खून और वो भी सबसे पुरानी दुश्मन ‘स्त्री’ का, लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा था. सारे वर्चस्व का खेल यहीं से तो शुरू होता है. बाकी दुश्मन तो बदलते रहते हैं, लेकिन स्त्री तो वह तो दुश्मन है, जिसके प्रति हम सबके भीतर ‘भोग्या’ होने का एक स्थाई भाव है.
रेप के चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद लोगो पुलिस पर फूलों की वर्षा करते हैं. हर तरफ से पुलिस की सराहना में नारे गढ़े जाते हैं. सत्ता के साथ-साथ विपक्ष भी पुलिस की प्रशंसा में कसीदे काढ़ता है. आखिर लड़ाई उस दौर में है, जहाँ मनुष्यों को भी बचे रहने के लिए अपने को अर्ध संक्रमित बताना ही पड़ता है, या फिर उन्हीं फिल्मों की तरह कुछ अर्द्धसंक्रमित ही, मनुष्यों को नेतृत्व प्रदान करने आगे आते हैं.
तो सवाल उठता कि लोग क्या करें? जब भी ऐसे मुश्किल सवालों से सामना होता है, तो जवाब ढूंढने उसी अधनंगे फ़क़ीर के पास जाना पड़ता है, जो कहता है कि पाप को मारो, पापी को नहीं. असली ड्रैकुला तो वह विचारधारा है, और उसे मारने के लिए, उसका सीना जो कि यह बाज़ार और उसका मीडिया है, उसको भेदना होगा. लेकिन हमें अपने आप को आइने में गौर से देखना सबसे ज्यादा ज़रूरी है. हमारे नेताओं को अहिंसा और अपरिग्रह में अपनी आस्था फिर दिखानी होगी और नेतृत्व के ढूंढ के लाना होगा.