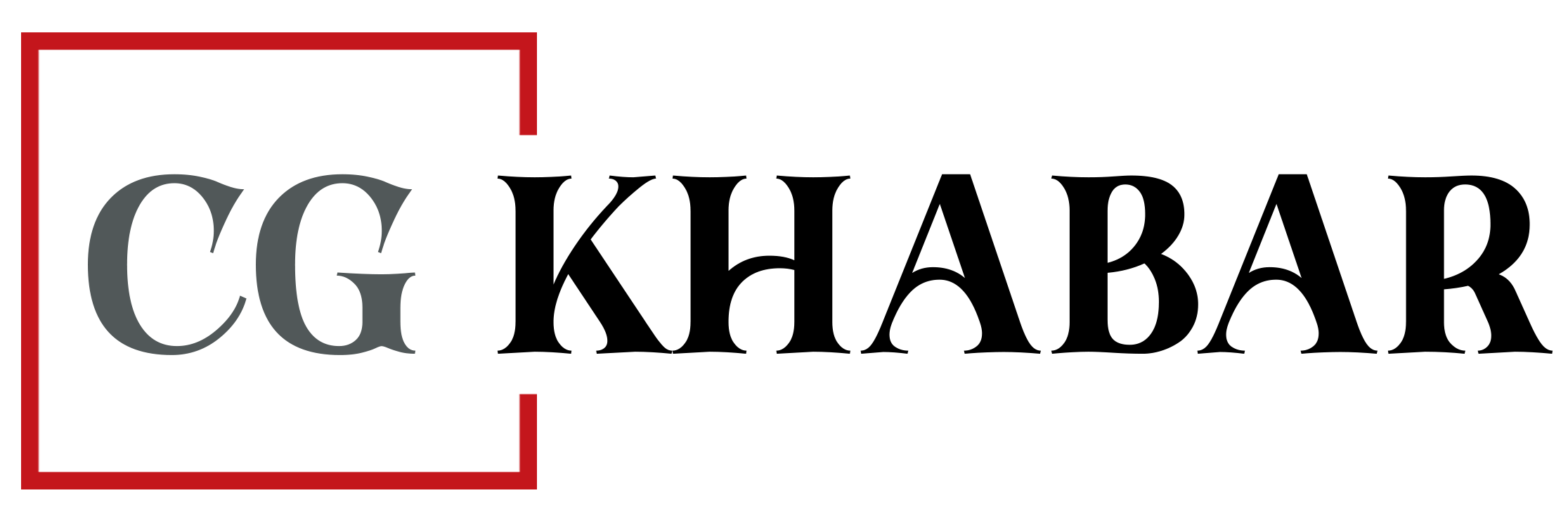न्यूटन : साधारण की महिमा
पुरुषोत्तम अग्रवाल | फेसबुक: कल रात इंटरनेट पर खबर देखी, ‘न्यूटन’ ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गयी, जाहिर है कि चयन समिति को विदेशी भाषा कैटेगरी के लिए इससे बेहतर मिल गयीं होंगी. लेकिन यह खबर पढ़ कर अफसोस तो हुआ. तीन महीने पहले जब यह फिल्म देखी थी, तो मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था. तब से लगातार ताज्जुब भी होता रहा कि इस फिल्म पर उतनी बात क्यों नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी.
नहीं, गलत कहा मैंने. ताज्जुब नहीं हुआ, मैं जानता था कि न्यूटन पर हाइप बनने का सवाल ही नहीं. ऐसा नहीं कि तारीफ नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे लगता रहा है कि उस उत्साह के साथ फिल्म को रिसीव नहीं किया गया जिसकी वह हकदार है. वजह शायद यह है-यह फिल्म अस्मिता के नहीं व्यवस्था के मुहावरे में बात करती है. ठीक यही स्थिति बांबे वेल्वेट के साथ हुई थी.
मतलब यह नहीं सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता न्यूटन के लिए महत्वपूर्ण नहीं. मतलब यह कि न्यूटन के निर्देशक अमित मसूरकर और लेखक मयंक तिवारी जानते हैं कि अस्मिताओं के सवाल व्यवस्था और मूलभूत सामाजिक संरचना के प्रति सचेत रहते हुए ही सही ढंग से उठाए जा सकते हैं.
न्यूटन आदिवासियों की विडंबना के बारे में बहुत अनाटकीय, और इसीलिए बहुत मार्मिक ढंग से बात करती है. एक तरफ माओवादियों की, दूसरी तरफ सरकार की ताकत के बीच पिसते आदिवासियों की हालत यह है कि वे न आशावादी है, न निराशावादी; वे सिर्फ आदिवासी हैं. इस विडंबना को बताने वाले शब्द किसी नाटकीय ढंग से नहीं, बल्कि वक्तकटी के लिए चल रही गप-शप के बीच दर्शक तक पहुँचते हैं. इस गप-शप के दौरान न्यूटनकुमार का सवाल है-‘मालको, आप आशावादी हैं, या निराशावादी’ . मालको का उत्तर फौरन आता है, “मैं आदिवासी हूँ”.
एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ माओवादी, पृष्ठभूमि में विकास की वह विकृत कल्पना जिसमें नेता वादा करते हैं-बच्चों के एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में लैपटाप थमाने का, लोकनाथजी ( रघुवीर यादव) आदिवासियों के बीच वोटिंग को पापुलर बताने की राह खोजते हैं-घर-घर टीवी पहुँचाने में, ताकि वे शानदार चीजें देख कर विकास के लिए ललचाने लगें, वोट देने लगें. फिल्म समाप्त होने के जरा पहले ही हम देखते हैं भीमकाय मशीनें, तेजी से बनती हुई सड़क…गांव के स्कूल की हालत, गांव वालों के जले हुए घर हम पहले ही देख चुके हैं. विलायती पत्रकारों के सामने वोट डालने के लिए हाँका लगा कर, घेर कर निकाले गये आदिवासियों से भी हमारी भेंट फिल्म के दौरान हो चुकी है. अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी ड्यूटी बजा रहे न्यूटनकुमार और कमांडेंट आत्मासिंह को भी हम देख चुके हैं–इन सब चीजों को देख चुकने के बाद, ऐन आखिर में “विकास” लाने वाली ये भीमकाय मशीनें एक रूपक बनाती हैं, उस व्यवस्था का, जिसमें सच्चाई और ईमानदारी की जगह दिनोंदिन सिकुड़ती जा रही है.
अमित मसूरकर और उनकी टीम ने इस फिल्म में कई कमाल किये हैं. एक तो खामोशी का इस्तेमाल. फिल्मों में आम तौर से बैकग्राउंड संगीत के जरिए असर बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मसूरकर का ज्यादा भरोसा संवादों पर, उससे भी ज्यादा खामोशी पर है. ऐसे कई दृश्य फिल्म में हैं जहाँ मसूरकर खामोशी के जरिए दर्शक से बात करते हैं. खामोशी-आशा-निराशा के परे जाने के लिए मजबूर कर दिये गये आदिवासियों की. खामोशी-उस पूरे लैंडस्केप की, जिसमें आप पात्रों को बात करते सुन रहे हैं, देख रहे हैं. इसी के साथ, विकास के पागलपन और व्यवस्था की अंतर्निहित भयानकता का नैरेशन करने में मसूरकर ने जिस संयम से, कमसुखनी से काम लिया है, वह लाजबाव है. पूरी फिल्म एक बड़े “साधारण” ढर्रे पर चल रही “जिन्दगी” का बयान है. अंत भी, किसी परिणति को बताता ‘दि एंड’ नहीं, बल्कि गोया यह कहता अल्प-विराम है कि पिक्चर अभी बाकी है.
शुरु में ही फिल्म स्थापित कर देती है कि आदर्शवादी व्यक्ति की समस्या उसकी ईमानदारी नहीं बल्कि ईमानदार होने का घमंड है. फिल्म कहना यह चाहती है कि अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, देश प्रगति करता जाएगा. लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते फिल्म का यह संदेश खोखला नहीं तो अधूरा जरूर लगने लगता है. यह सही है कि हर व्यक्ति को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसकी उपयोगिता सीमित है, यदि पूरी व्यवस्था और उसके तंत्र के बारे में किसी तरह की समग्र समझ आपके पास न हो.
फिल्म की अपनी ईमानदारी इस बात में है कि वह इस तरह की किसी समग्र समझ का निराधार दावा नहीं करती. इस तरह यह फिल्म हमारे उत्तर-आधुनिक, सत्यातीत ( पोस्ट ट्रुथ) का कनफेशन भी बन जाती है. गलत हो रहा है, विकास की धारणा विकृत हो चुकी है, जो पिस रहे हैं वे आशा-निराशा में फर्क करने की जरूरत तक नहीं महूसूस नहीं करते, लेकिन कोई “सूरत नजर नहीं आती”. फिर भी फिल्म यह कहने तक नहीं पहुँचती कि, “ कोई उम्मीद बर नहीं आती”.
यह सही है कि जब तक एक समग्र नजरिये को हम हासिल न कर लें तब तक हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठा जा सकता. उस खोज को जारी रखते हुए ही, अपना काम तो ईमानदारी से करना ही है. हालाँकि “ईमानदारी” का एक अर्थ वह भी हो सकता है जो कमांडेंट आत्मासिंह लेते हैं, किसी तरह चुनाव की औपचारिकता पूरी करा देना! दूसरी तरफ न्यूटन कुमार (राजकुमार राव ) हैं जिन्होंने अपना नाम बदल कर नूतन से न्यूटन कर लिया है. राजकुमार राव ने इस चरित्र को बखूबी निभाया है, एक बार फिर से रेखांकित किया है कि वे कितने बेहतरीन अभिनेता हैं.
शुरु में ही चुनाव आयोग का अफसर (संजय मिश्रा) न्यूटन को अहसास करता है कि इस नाम के जरिए उन्होंने कितनी भारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है-‘ न्यूटन के पहले माना जाता था कि जमीन का कानून अलग है, आसमान का अलग. न्यूटन ने दुनिया को बताया कि कुदरत का कानून एक ही है. पहाड़ से अंबानी गिरे या चाय वाली-नतीजा एक ही होगा.’
न्यूटन का काम केवल भौतिकी तक सीमित ना रहकर सामाजिक संबंधों, प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों को नये सिरे से परिभाषित करने तक जाता है, उनकी खोज आधुनिक सोच की शुरुआत को रेखांकित करती है-इस बात को इतने सहज ढंग से कहने वाले निर्देशक और संवाद -लेखक से भविष्य के लिए वाकई और भी उम्मीद की जा सकती है.
फिल्म में विभिन्न रोल निभा रहे कलाकारों ने अपने-अपने चरित्रों को नहीं, फिल्म के कथानक के मर्म को भी समझा है. इसीलिए अति-नाटकीयता की कहीं न जरूरत है न गुंजाइश. इस लिहाज से आत्मासिंह का चरित्र और पंकज त्रिपाठी द्वारा उसका निर्वाह खास तौर से ध्यान खींचता है. वह कोई करप्ट अफसर नहीं, यह स्थापित करने के लिए आखिर में एक सीन रचा गया है जिसमें खरीदारी कर रहे उसके परिवार को साढ़े तीन हजार रुपयों का बिल कुछ ज्यादा लगने लगता है. पूरी फिल्म में पंकज ने जिस तरह, अंडर-स्टेटमेंट के जरिए इस चरित्र को उंकेरा है, वह याद रहेगा. हर दृश्य में जिस तरह वे अपने चेहरे से, आवाज से, और बॉडी-मूवमेंट से विडंबना को रेखांकित करते हैं, उससे एक बात चरित्र के बारे में मालूम पड़ती है, और एक अभिनेता के बारे में.
आत्मासिंह निजी तौर पर ईमानदार भी है, संवेदनशील भी. लेकिन पुलिस की नौकरी में कमाए अनुभवों के कारण उन्होंने इन गुणों की सीमाएँ भी देख ली हैं, और व्यवस्था की अकूत जटिलता भी. ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वभाव में जो स्थायी विडंबना-बोध आ जाता है, उसे जीना तो किसी का स्वभाव बन सकता है, लेकिन किसी अभिनेता द्वारा इस स्थायी विडंबना-बोध को निहायत अंडर-स्टेटेड तरीके से निरंतर संप्रेषित कर पाना बहुत बड़ा कमाल है जो पंकज ने कर दिखाया है.
न्यूटन जरूर-जरूर देखने लायक फिल्म है. बार-बार देखने लायक फिल्म है. निर्देशक, अभिनेता, लेखक सबसे और ज्यादा उम्मीद जगाने वाली फिल्म है. आपने अब तक नहीं देखी तो चूकिए मत, देख डालिए.